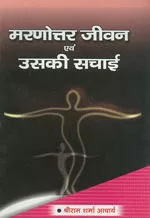|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> मरणोत्तर जीवन एवं उसकी सचाई मरणोत्तर जीवन एवं उसकी सचाईश्रीराम शर्मा आचार्य
|
184 पाठक हैं |
||||||
क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है ?
घास-पात की तरह मनुष्य भी माता के पेट से जन्म लेता है, पेड़-पौधों की तरह
बढ़ता है और पतझड़ में पीले पत्तों की तरह जरा-जीर्ण होकर मौत के मुँह में
चला जाता है। देखने में तो मानवी सत्ता का यही आदि-अन्त है। प्रत्यक्षवाद
की सचाई वहीं तक सीमित है, जहाँ तक इंद्रियों या उपकरणों से किसी पदार्थ
को देखा-नापा जा सके। इसलिए पदार्थ विज्ञानी जीवन का प्रारम्भ व समाप्ति
रासायनिक संयोगों एवं वियोगों के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मनुष्य एक
चलता-फिरता पेड़-पादप भर है। लोक-परलोक उतना ही है जितना कि काया का
अस्तित्व। मरण के साथ ही आत्मा अथवा काया सदा-सर्वदा के लिए समाप्त हो
जाती है।
बात दार्शनिक प्रतिपादन या वैज्ञानिक विवेचन भर की होती तो उसे भी अन्यान्य उलझनों की तरह पहेली, बुझौवल समझा जा सकता था और समय आने पर उसके सुलझने की प्रतीक्षा की जा सकती थी। किन्तु प्रसंग ऐसा है जिसका मानवी दृष्टिकोण और समाज के गठन, विधान और अनुशासन पर सीधा प्रभाव पढ़ता है। यदि जीवन का आदि-अंत-जन्म-मरण तक ही सीमित है, तो फिर इस अवधि में जिस भी प्रकार जितना भी मौज-मजा उड़ाया जा सकता हो, क्यों न उड़ाया जाए ?
दुष्कृत्यों के फल से यदि चतुरतापूर्वक बचा जा सकता है, तो पीछे कभी उसका दंड़ भुगतना पड़ेगा, ऐसा क्यों सोचा जाए ? अनास्था की इस मनोदशा में पुण्य-परमार्थ का, स्नेह-सहयोग का भी कोई आधार नहीं रह जाता। तब मत्स्य-न्याय अपनाने, जंगल का कानून बरतने और ‘‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’’ की मान्यता का सहज ही बोलबाला होता है। यह जीवन दर्शन मनुष्य को नैतिक अराजकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। समाज के प्रति निष्ठावान रहने की तब कोई आवश्यकता तक प्रतीत नहीं होती।
चर्चा मृत्यु एवं मरणोत्तर जीवन के संबंध में चल रही है। मृत्यु के संबंध में भिन्न-भिन्न धर्मो की भिन्न-भिन्न धाराणाएँ हैं। लेकिन एक विषय में सभी एकमत हैं कि मृत्यु का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। इसी आधार पर कुछ धर्मों ने मरने के बाद फिर से जन्म लेने की मान्यता को स्वीकार किया है और कुछ ने मतानुसार मृत्यु एक ऐसी घटना है, जिसमें चेतना या प्राण सदा के लिए सो जाते हैं और सृष्टि के अंत में फिर जाग उठते हैं। इस दृष्टि से आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को अन्यान्य धर्मों ने भी स्वीकार किया है, लेकिन यह सिद्धान्त भारतीय दर्शन का तो प्राण ही है।
भारतीय दर्शन के अनुसार पुर्नजन्म की मान्यता के साथ कर्मफल का सघन संबंध है। जिन्हें भले या बुरे कर्मों का परिणाम तत्काल नहीं मिल सका, उन्हें अगले जन्म में कर्मफल भोगना पड़ता है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने पर पापफल और दुष्कर्मों के दंड से डरने तथा पुण्यकाल के प्रति आश्वस्त रहने की मन:स्थिति बनी रहती है। फलत: पुनर्जन्म के मानने वालों को अपने कर्मों का स्तर सही रखने की आवश्यकता अनुभव होती है और तत्काल फल न मिलने से किसी प्रकार की उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होती। पिछले दिनों भौतिक विज्ञान की प्रगति से उत्पन्न हुए उत्साह के कारण यह कहा जाने लगा कि सत्य केवल उतना ही है, जितना कि प्रयोगशाला में सिद्ध हो सके। जो प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वह सत्य नहीं है।
चूँकि चेतना को प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष नहीं किया जा सका इसलिए घोषित कर दिया कि शरीर की आत्मा है और मृत्यु के बाद उसका सदा-सर्वदा के लिए अंत हो जाता है। इस घोषणा के अनुसार मनुष्य को चलता-फिरता पौधा भर कहा गया, जो उगता है और सूखकर समाप्त हो जाता है। यह मान्यता पक्ष एक सिद्धान्त या प्रतिपादन भर बनकर नहीं रह सकती, उसकी प्रतिक्रिया चिंतन और चरित्र पर भी होती है। पुनर्जन्म, कर्मफल, परलोक और पाप-पुण्य की आस्था जिस प्रकार व्यक्ति को दुष्कर्मों से बचाए रहती है, उसी प्रकार शरीर को ही सत्य और आत्मा को मिथ्या मान लिया जाए, तो लगता है कि पाप-पुण्य के पचड़े में पड़ने से क्या लाभ ? चतुरता के बल पर जितना भी संभव हो सके, स्वार्थ सिद्ध किया जाना चाहिए।
अब जो प्रमाण सामने आए हैं और उनकी वैज्ञानिक गवेषणाएँ की गई हैं, उनके अनुसार यह भ्रम ढहता जा रहा है कि जीवन-चेतना का अस्तित्व शरीर तक ही सीमित है। इस धारणा में भ्रम तो पहले भी विद्यमान था, पर अब इस सचाई के प्रमाणों पर भी वैज्ञानिक ध्यान देने लगे हैं कि पुनर्जन्म वास्तव में एक ध्रुव सत्य है। पुर्नजन्म के सिद्धान्त की पुष्टि करने वाले अनेकानेक प्रमाण आ रहे हैं। भारत में तो इस संबंध में चिरकाल से प्रचलित विश्वास के कारण यह कहा जाता रहा कि पुनर्जन्म की स्मृति बताने वाले यहाँ के वातावरण से प्रभावित रहे होंगे या किसी कल्पना की आधी-अधूरी पुष्टि हो जाने पर यह घोषित किया जाता होगा कि यह बालक पिछले जन्म में अमुक था। यद्यपि इस तरह के प्रकरणों में जिस कठोरता के साथ जाँच-पड़ताल की गई, उससे यह आशंका अपने आप ही निरस्त हो जाती थी। उदाहरण के लिए पिछले जन्म के संबंधियों के नाम और रिश्ते बताने, ऐसी घटनाओं का जिक्र करने जिनकी जानकारी दूरस्थ व्यक्तियों को भी नहीं रही, नितांत व्यक्तिगत और पति-पत्नी तक ही सीमित बातों को बता देने, पिछले जन्म में जमीन में गाड़ी गई चीज उखाड़कर देने तथा अपने और पराये खेतों का विवरण बताने जैसे अनेक संदर्भ ऐसे हैं, जिनके आधार पर पुनर्जन्म की प्रामाणिकता से इनकार नहीं किया जा सकता।
बात दार्शनिक प्रतिपादन या वैज्ञानिक विवेचन भर की होती तो उसे भी अन्यान्य उलझनों की तरह पहेली, बुझौवल समझा जा सकता था और समय आने पर उसके सुलझने की प्रतीक्षा की जा सकती थी। किन्तु प्रसंग ऐसा है जिसका मानवी दृष्टिकोण और समाज के गठन, विधान और अनुशासन पर सीधा प्रभाव पढ़ता है। यदि जीवन का आदि-अंत-जन्म-मरण तक ही सीमित है, तो फिर इस अवधि में जिस भी प्रकार जितना भी मौज-मजा उड़ाया जा सकता हो, क्यों न उड़ाया जाए ?
दुष्कृत्यों के फल से यदि चतुरतापूर्वक बचा जा सकता है, तो पीछे कभी उसका दंड़ भुगतना पड़ेगा, ऐसा क्यों सोचा जाए ? अनास्था की इस मनोदशा में पुण्य-परमार्थ का, स्नेह-सहयोग का भी कोई आधार नहीं रह जाता। तब मत्स्य-न्याय अपनाने, जंगल का कानून बरतने और ‘‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’’ की मान्यता का सहज ही बोलबाला होता है। यह जीवन दर्शन मनुष्य को नैतिक अराजकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। समाज के प्रति निष्ठावान रहने की तब कोई आवश्यकता तक प्रतीत नहीं होती।
चर्चा मृत्यु एवं मरणोत्तर जीवन के संबंध में चल रही है। मृत्यु के संबंध में भिन्न-भिन्न धर्मो की भिन्न-भिन्न धाराणाएँ हैं। लेकिन एक विषय में सभी एकमत हैं कि मृत्यु का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। इसी आधार पर कुछ धर्मों ने मरने के बाद फिर से जन्म लेने की मान्यता को स्वीकार किया है और कुछ ने मतानुसार मृत्यु एक ऐसी घटना है, जिसमें चेतना या प्राण सदा के लिए सो जाते हैं और सृष्टि के अंत में फिर जाग उठते हैं। इस दृष्टि से आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को अन्यान्य धर्मों ने भी स्वीकार किया है, लेकिन यह सिद्धान्त भारतीय दर्शन का तो प्राण ही है।
भारतीय दर्शन के अनुसार पुर्नजन्म की मान्यता के साथ कर्मफल का सघन संबंध है। जिन्हें भले या बुरे कर्मों का परिणाम तत्काल नहीं मिल सका, उन्हें अगले जन्म में कर्मफल भोगना पड़ता है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने पर पापफल और दुष्कर्मों के दंड से डरने तथा पुण्यकाल के प्रति आश्वस्त रहने की मन:स्थिति बनी रहती है। फलत: पुनर्जन्म के मानने वालों को अपने कर्मों का स्तर सही रखने की आवश्यकता अनुभव होती है और तत्काल फल न मिलने से किसी प्रकार की उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होती। पिछले दिनों भौतिक विज्ञान की प्रगति से उत्पन्न हुए उत्साह के कारण यह कहा जाने लगा कि सत्य केवल उतना ही है, जितना कि प्रयोगशाला में सिद्ध हो सके। जो प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वह सत्य नहीं है।
चूँकि चेतना को प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष नहीं किया जा सका इसलिए घोषित कर दिया कि शरीर की आत्मा है और मृत्यु के बाद उसका सदा-सर्वदा के लिए अंत हो जाता है। इस घोषणा के अनुसार मनुष्य को चलता-फिरता पौधा भर कहा गया, जो उगता है और सूखकर समाप्त हो जाता है। यह मान्यता पक्ष एक सिद्धान्त या प्रतिपादन भर बनकर नहीं रह सकती, उसकी प्रतिक्रिया चिंतन और चरित्र पर भी होती है। पुनर्जन्म, कर्मफल, परलोक और पाप-पुण्य की आस्था जिस प्रकार व्यक्ति को दुष्कर्मों से बचाए रहती है, उसी प्रकार शरीर को ही सत्य और आत्मा को मिथ्या मान लिया जाए, तो लगता है कि पाप-पुण्य के पचड़े में पड़ने से क्या लाभ ? चतुरता के बल पर जितना भी संभव हो सके, स्वार्थ सिद्ध किया जाना चाहिए।
अब जो प्रमाण सामने आए हैं और उनकी वैज्ञानिक गवेषणाएँ की गई हैं, उनके अनुसार यह भ्रम ढहता जा रहा है कि जीवन-चेतना का अस्तित्व शरीर तक ही सीमित है। इस धारणा में भ्रम तो पहले भी विद्यमान था, पर अब इस सचाई के प्रमाणों पर भी वैज्ञानिक ध्यान देने लगे हैं कि पुनर्जन्म वास्तव में एक ध्रुव सत्य है। पुर्नजन्म के सिद्धान्त की पुष्टि करने वाले अनेकानेक प्रमाण आ रहे हैं। भारत में तो इस संबंध में चिरकाल से प्रचलित विश्वास के कारण यह कहा जाता रहा कि पुनर्जन्म की स्मृति बताने वाले यहाँ के वातावरण से प्रभावित रहे होंगे या किसी कल्पना की आधी-अधूरी पुष्टि हो जाने पर यह घोषित किया जाता होगा कि यह बालक पिछले जन्म में अमुक था। यद्यपि इस तरह के प्रकरणों में जिस कठोरता के साथ जाँच-पड़ताल की गई, उससे यह आशंका अपने आप ही निरस्त हो जाती थी। उदाहरण के लिए पिछले जन्म के संबंधियों के नाम और रिश्ते बताने, ऐसी घटनाओं का जिक्र करने जिनकी जानकारी दूरस्थ व्यक्तियों को भी नहीं रही, नितांत व्यक्तिगत और पति-पत्नी तक ही सीमित बातों को बता देने, पिछले जन्म में जमीन में गाड़ी गई चीज उखाड़कर देने तथा अपने और पराये खेतों का विवरण बताने जैसे अनेक संदर्भ ऐसे हैं, जिनके आधार पर पुनर्जन्म की प्रामाणिकता से इनकार नहीं किया जा सकता।
पुनर्जन्म सिद्धांत को भली भाँति समझा जाए
किसी भी सिद्धांत को भली भाँति नहीं समझा जाए, तो उसे मानने का दम भरने पर
भी आचरण उससे विपरीत ही बना रहता है। पुनर्जन्म सिद्धान्त के साथ भी ऐसा
ही हुआ है। उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया को न समझने वालों ने जहाँ इस जीवन
में भौतिक सुविधा-साधनों को ही पूरी तरह पिछले जन्म के पुण्यफल मान लिया,
वहीं इस पुण्य कर्म का अर्थ पूजा-स्त्री, कर्मकांड तक ही सीमित माना जाने
लगा। परिणाम यह हुआ कि न तो व्यक्ति की आदर्शपरायणता के प्रति कोई
वास्तविक सम्मान बचा, न ही पुरुषार्थ की प्रगति का आधार समझा गया। इसके
स्थान पर भौतिक सुख-सुविधाएँ अपने पुरुषार्थ की तुलना में कहीं अधिक जुटा
पाना या पा जाना ही चारित्रिक सौभाग्य या श्रेष्ठता का प्रमाण माना जाने
लगा और वह श्रेष्ठता पाने का आसान तरीका ग्रह-नक्षत्रों, देवताओं को
टंट-टंट से प्रसन्न करना समझा गया।
यह एक विचित्र विडंबना ही है कि पुनर्जन्म का जो सिद्धान्त पुरुषार्थ और कर्म की महत्ता का प्रतिपादक था, कठिन-से-कठिन अप्रत्याशित विपत्ति को भी प्रारब्ध भोग मानकर धैर्यपूर्वक सहने और आगे उत्कर्ष हेतु पूर्ण विश्वास के साथ प्रयासरत रहने की प्रेरमा देता था, वही निष्क्रियता और अंध नियतिवाद का भ्रांत मतवाद बनकर रह गया है।
मनुष्य द्वारा अपने भाग्य का निर्माण आप किए जाने का तथ्य भुलाकर यह माना जाने लगा कि देवता अपनी मरजी और मौज के मुताबिक किसी का भाग्य खराब, किसी का अच्छा सिखते या बनाते हैं। भला यदि ऐसा होने लगे, तो इन देवताओं को शक्ति-संपन्न पागलों के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा ? पूजा-स्त्री के रूप में मिथ्या या अतिरंजित प्रशंसा तथा अत्यंत सस्ती उपहार-सामग्री पाकर ही अपनी नीति-व्यवस्था को उलट-पलट देने वाले देवता तो अस्त-व्यस्त अफसरों और बाबुओं से भी अधिक भौंदू सिद्ध होते।
प्राय: किसी को धन-सुविधासंपन्न देखकर इसे उसके पिछले जन्मों का पुण्य मान लिया जाता है। पर, धन मनुष्य की अनेक विभूतियों में से एक विभूति है, एकमात्र नहीं। कोई व्यक्ति धनी है, यह यदि उसके विगत पुण्य का फल है, किन्तु साथ ही यदि वह दुराचारी है, क्षुद्र है, क्रूर है, व्यसनी है; तो यह सब उसके किसी विगत पाप का फल मानना होगा। यही स्वाभाविक और तर्कसंगत प्रतिपादन कहलाएगा। सामान्यत: लोग जीवन में कुछ सत्कर्म करते हैं, कुछ अनैतिकता भी।
यह एक विचित्र विडंबना ही है कि पुनर्जन्म का जो सिद्धान्त पुरुषार्थ और कर्म की महत्ता का प्रतिपादक था, कठिन-से-कठिन अप्रत्याशित विपत्ति को भी प्रारब्ध भोग मानकर धैर्यपूर्वक सहने और आगे उत्कर्ष हेतु पूर्ण विश्वास के साथ प्रयासरत रहने की प्रेरमा देता था, वही निष्क्रियता और अंध नियतिवाद का भ्रांत मतवाद बनकर रह गया है।
मनुष्य द्वारा अपने भाग्य का निर्माण आप किए जाने का तथ्य भुलाकर यह माना जाने लगा कि देवता अपनी मरजी और मौज के मुताबिक किसी का भाग्य खराब, किसी का अच्छा सिखते या बनाते हैं। भला यदि ऐसा होने लगे, तो इन देवताओं को शक्ति-संपन्न पागलों के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा ? पूजा-स्त्री के रूप में मिथ्या या अतिरंजित प्रशंसा तथा अत्यंत सस्ती उपहार-सामग्री पाकर ही अपनी नीति-व्यवस्था को उलट-पलट देने वाले देवता तो अस्त-व्यस्त अफसरों और बाबुओं से भी अधिक भौंदू सिद्ध होते।
प्राय: किसी को धन-सुविधासंपन्न देखकर इसे उसके पिछले जन्मों का पुण्य मान लिया जाता है। पर, धन मनुष्य की अनेक विभूतियों में से एक विभूति है, एकमात्र नहीं। कोई व्यक्ति धनी है, यह यदि उसके विगत पुण्य का फल है, किन्तु साथ ही यदि वह दुराचारी है, क्षुद्र है, क्रूर है, व्यसनी है; तो यह सब उसके किसी विगत पाप का फल मानना होगा। यही स्वाभाविक और तर्कसंगत प्रतिपादन कहलाएगा। सामान्यत: लोग जीवन में कुछ सत्कर्म करते हैं, कुछ अनैतिकता भी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book